केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) एक संवैधानिक निकाय नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र निकाय है, जो सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के तहत कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों आदि से संबंधित शिकायतों और अपीलों को देखता है। भारत सरकार के तहत उन व्यक्तियों की शिकायतों पर कार्रवाई करना, जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचना अनुरोध प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं।
केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में:-
केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) के प्रावधानों के तहत की गई थी । केंद्रीय सूचना आयोग शासन व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, उत्पीड़न और सत्ता के दुरुपयोग या दुरुपयोग को रोकने के लिए इस तरह की पारदर्शिता आवश्यक है।
केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना
केंद्रीय सूचना आयोग में केंद्रीय सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्त शामिल होते हैं। भारत के राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति उस समिति की सिफारिश पर करते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
उन्हें अनुभव और ज्ञान और कानून, प्रबंधन, पत्रकारिता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रशासन और शासन, मास मीडिया और सामाजिक सेवा के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। उन्हें किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधान सभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। उन्हें किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं होना चाहिए या कोई व्यवसाय नहीं करना चाहिए, उन्हें कोई लाभ का पद नहीं रखना चाहिए या कोई अन्य पेशा नहीं अपनाना चाहिए।
पढ़ेंः एशिया का सबसे पढ़ा-लिखा गांव कौन-सा है, जानें
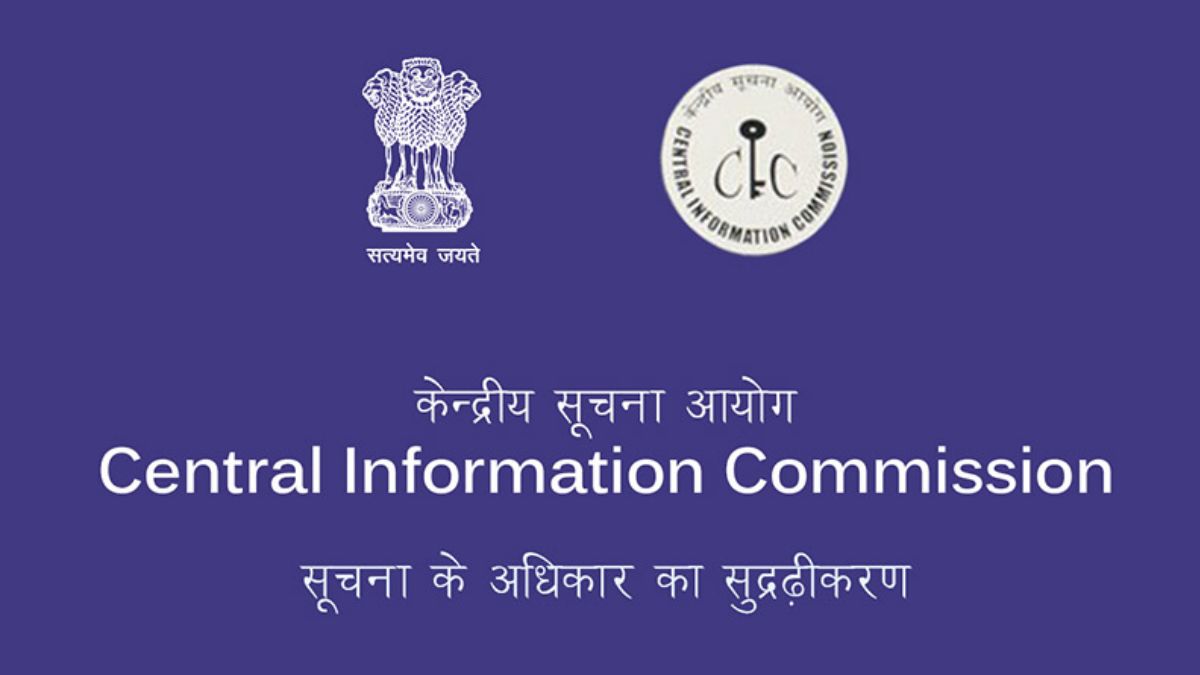
कार्यकाल एवं सेवा
मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त पांच साल तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रहते हैं । वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं हैं।
केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियां
केंद्रीय सूचना आयोग की शक्तियां और कार्य निम्नलिखित हैं:
-उचित आधार होने पर आयोग किसी भी मामले में जांच का आदेश दे सकता है।
-आयोग के पास सार्वजनिक प्राधिकरण से अपने निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करने की शक्ति है।
-यदि सार्वजनिक प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो आयोग ऐसी अनुरूपता को बढ़ावा देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश कर सकता है।
-किसी भी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करना और उसकी जांच करना आयोग का कर्तव्य है:
-जिसे निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपने सूचना अनुरोध का जवाब नहीं मिला है;
-जो सोचता है कि दी गई जानकारी अधूरी, भ्रामक या झूठी है और जानकारी प्राप्त करने से संबंधित कोई अन्य मामला है।
-जो जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण सूचना अनुरोध प्रस्तुत नहीं कर सका हो;
-जो सोचता है कि ली गई फीस अनुचित है;
-मांगी गई जानकारी को किसी ने अस्वीकार कर दिया है।
-किसी शिकायत की जांच के दौरान आयोग किसी भी रिकॉर्ड की जांच कर सकता है, जो सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में है और ऐसे किसी भी रिकॉर्ड को किसी भी आधार पर रोका नहीं जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें, तो जांच के दौरान सभी सार्वजनिक रिकॉर्ड जांच के लिए आयोग को दिए जाने चाहिए।
-जांच करते समय आयोग के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं।
-आयोग इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर केंद्र सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखती है।
सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई अधिनियम) इसलिए बनाया गया, ताकि सूचना मांगना सरल, आसान, समयबद्ध और सस्ता हो जाए, जिससे यह कानून सफल, शक्तिशाली और प्रभावी बन गया। आयोग की शक्तियां केवल सूचना देने तक ही सीमित हैं, विसंगतियां होने पर भी कोई कार्यवाही करने तक नहीं। आयोग के पास कर्मचारियों की कमी है और उस पर मामलों का अत्यधिक बोझ है।
आरटीआई अधिनियम केवल सरकारी संस्थानों पर लागू होता है, निजी उद्यमों पर नहीं। यहां तक कि बीसीसीआई जैसे कुछ सार्वजनिक संस्थान भी दावा करते हैं कि वे कानून के दायरे में नहीं आते हैं। राजनीतिक दल अपनी फंडिंग और अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी जनता के साथ साझा करने में अनिच्छुक हैं।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation